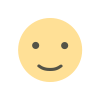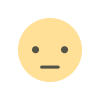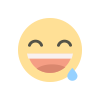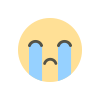उत्तराखंड के 25 साल: पहाड़ वही, दर्द वही…
आज उत्तराखंड अपनी रजत जयंती का सरकारी जश्न मना रहा है। चारों ओर विकास के दावों की गूँज है, पर यह गूँज पहाड़ के वीरान गाँवों की खामोशी में दब जाती है। 25 साल हो गए राज्य बने, 25 साल

जन-आंदोलन का अपमान और सत्ता का कारोबार
आज उत्तराखंड अपनी रजत जयंती का सरकारी जश्न मना रहा है। चारों ओर विकास के दावों की गूँज है, पर यह गूँज पहाड़ के वीरान गाँवों की खामोशी में दब जाती है। 25 साल हो गए राज्य बने, 25 साल में 10 मुख्यमंत्री (अस्थिरता का जीता जागता प्रमाण)। सत्ता की यह कुर्सी ऐसे घूमती रही, जैसे यह करोड़ों लोगों का भविष्य नहीं, बल्कि महज एक पासा हो, जिसके फेंकने से सिर्फ नेताओं की नियति बदलती है।
राज्य किसके लिए बना था? पहाड़ के लिए, या सत्ता की बंदरबाँट के लिए? सच्चाई यह है कि यह राज्य आंदोलन की पवित्र भावना को सत्ता के गलियारों में नेताओं का कारोबार बना दिया गया। जनता ने सड़कें, स्कूल, अस्पताल, और रोजगार माँगा था। मिला क्या? फाइलों की धूल, घोषणाओं के पहाड़, और टूटे हुए सपने। यह आरोप नहीं, यह पहाड़ की हर सूनी पगडंडी, हर बंद स्कूल, हर उजड़े गाँव की चीख है, जिसे आज हम उत्तराखंड नहीं, मजबूरीखण्ड कहने को विवश हैं।
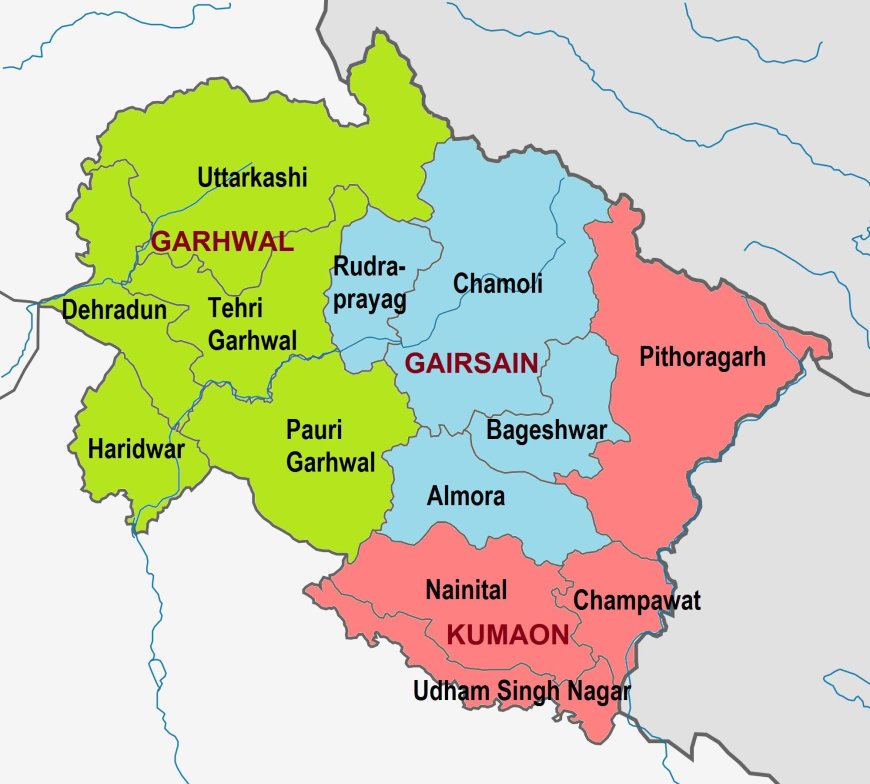
पलायन: पहाड़ का सबसे बड़ा जख्म—जब गांव केवल 'फोटो' में रह गए
पलायन उत्तराखंड के सीने का वह सबसे गहरा जख्म है, जो 25 साल में नासूर बन चुका है। राज्य आंदोलन के समय नारा था: "नौजवान पहाड़ छोड़कर नहीं जाएगा।" आज हकीकत देखिए:
आंकड़े बोलते हैं: पलायन आयोग (Migration Commission) के अनुसार, राज्य बनने के बाद से अब तक 5000 से ज्यादा गाँव पूरी तरह या आंशिक रूप से खाली हो चुके हैं। ये सिर्फ आँकड़े नहीं हैं, ये उन घरों के ताले हैं जिनमें अब कोई दीवाली नहीं जलती।
उजड़ा हुआ भूगोल: आज पहाड़ी गाँव की आबादी में सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएँ और मवेशी ही शेष हैं। युवा पीढ़ी—हमारी सबसे बड़ी मानव पूंजी—देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली, गुजरात, या खाड़ी देशों में 'मजबूरी' का जीवन जी रही है।
खेत झाड़ियों के हवाले: जिस धरती को सींचने के लिए अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई, वह आज बंजर, झाड़ियों के हवाले है। मन पहाड़ पर रहता है, पर शरीर को शहर में बेचना पड़ता है, क्योंकि यहां काम नहीं, सपने नहीं, सिस्टम नहीं है। सरकारी नीतियाँ सिर्फ पलायन को 'गिनती' हैं, उसे 'रोकती' नहीं।
स्वास्थ्य का व्यंग्य: एम्स की तस्वीर और खाट पर सफर
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति नेताओं और जनता के बीच की विशाल खाई को दर्शाती है। नेता अपनी हल्की सी अस्वस्थता पर हेलीकॉप्टर से उच्च स्तरीय अस्पताल जाते हैं। दूसरी ओर, गाँव की एक गर्भवती बहू, रात के अंधेरे में प्रसव पीड़ा झेलती हुई, खाट पर लादकर 8 किमी नीचे सड़क तक लाई जाती है—यह आज भी एक सामान्य पहाड़ी दृश्य है।
AIIMS की चमक: शहरों में एम्स की शानदार तस्वीरें चमकती हैं, पर पहाड़ के दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में न डॉक्टर हैं, न दवाइयाँ, और न ही आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा।
आयुष्मान कार्ड: एक 'टूटती हुई' उम्मीद: सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिए हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों के लिए यह अक्सर इलाज नहीं, केवल उम्मीद का एक टुकड़ा साबित होता है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का ढाँचा पूरी तरह से चरमरा चुका है।
व्यंग्य: पहाड़ों की स्वास्थ्य सेवाएँ ऐसी हैं कि यहाँ बीमारी से ज्यादा खतरा बीमार होने के बाद अस्पताल तक पहुँचने में है।
शिक्षा: मास्टर राजधानी में, बच्चे स्कूल में नहीं
कागजों में उत्तराखंड को 'शिक्षा वाला राज्य' कहा जाता है, पर धरातल पर शिक्षा सिर्फ एक और विफलता की कहानी है।
शिक्षकों का पलायन: पहाड़ के स्कूलों में शिक्षक टिकना नहीं चाहते। वे किसी भी कीमत पर अपनी पोस्टिंग राजधानी (देहरादून) या मैदानी क्षेत्रों में करवा लेते हैं। पहाड़ के स्कूल अक्सर अतिथि शिक्षकों या 'राम भरोसे' चलते हैं।
बंद और खाली स्कूल: कई पहाड़ी स्कूलों में 12-15 बच्चों की कक्षा होती है, जबकि कई स्कूलों में सिर्फ घंटी और ताला ही बजता है। राज्य बनने का सपना था कि पहाड़ में उच्च शिक्षा और IIT जैसी तकनीकी सोच आएगी।
निजी बनाम सरकारी: सरकारी स्कूल आज 'विकल्प' नहीं, बल्कि मजबूरी बन चुके हैं, जहाँ अभिभावक बच्चों को तभी भेजते हैं जब उनके पास निजी स्कूलों की भारी फीस देने का कोई रास्ता न हो। यह शैक्षिक असमानता भविष्य की पीढ़ियों को तबाह कर रही है।
सड़कें: टनल, हाईवे और गाँव की टूटती उम्मीद
हाईवे और टनल का निर्माण शानदार उपलब्धि है, जिसने पर्यटन को रफ्तार दी है। लेकिन यह विकास 'दिखावटी विकास' है, जो जनता की असली जरूरत से कोसों दूर है।
गाँव की सड़क का दर्द: बड़े हाईवे चमक रहे हैं, पर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पक्की गलियाँ आज भी सपना हैं। ये सड़कें अक्सर बरसात में टूट जाती हैं, और आपदा में सबसे पहले यही सड़कें लोगों की उम्मीद को तोड़ती हैं।
सरकारी पोस्ट बनाम हकीकत: सरकारी पोस्ट "कनेक्टिविटी मेजर अचीवमेंट" का गुणगान करती है, पर गाँव का बुजुर्ग सही बोलता है: "सड़क बनी है, पर गांव से अब लोग गिरे जाते हैं, लौटते नहीं।" क्योंकि सड़क ने शहर तक पहुँच आसान कर दी है, गांव को नहीं जोड़ा है।
निराशा नहीं, अब दिशा चाहिए
पिछले 25 सालों का सार यही है: नीचे भरा, ऊपर बहा। जो नेता जागा, उसने लूटा; जो जनता सोई, वो भूली। नेताओं ने फॉर्च्यूनर से फॉर्च्यून टावर तक का सफर तय किया और राजनीति को नौकरी नहीं, कारोबार बना दिया।
लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई है। पहाड़ हार नहीं मानता। यह सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार का गुस्सा नहीं है, यह उस माँ का दर्द है जिसके बेटे वापस नहीं लौटे।
अब जरूरत है: बड़े-बड़े दावे नहीं, छोटे-छोटे सच्चे कदम।
प्रदीप फुटेला
वरिष्ठ पत्रकार,संपादक कुमाऊं केसरी



 News Desk
News Desk